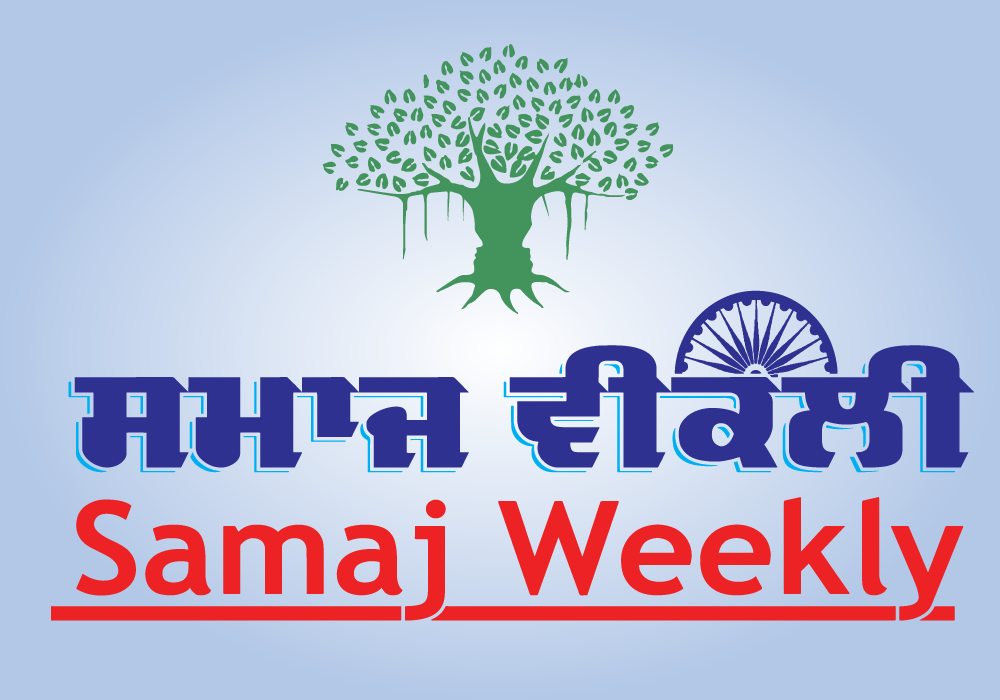समाज वीकली
राजेश चन्द्रा
 (माघ पूर्णिमा के दिन भगवान ने अनत्त सञ्ञ सुत्त का संगायन किया था और इसी पूर्णिमा के दिन वैशाली के चापाल चैत्य में भगवान ने सकल जगत को स्तब्ध कर देने वाली घोषणा की थी- तीन माह बाद तथागत महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होंगे। और माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रैदास का जन्म हुआ है। जन्म भी वहाँ हुआ जहाँ तथागत ने प्रथम धम्मोपदेश किया, वाराणसी में। संत रैदास बुद्ध धम्म की एक धारा हैं। संत रैदास जयंती के अवसर पर दिया गया एक व्याख्यान पुनः उद्धृत कर रहा हूँ।)
(माघ पूर्णिमा के दिन भगवान ने अनत्त सञ्ञ सुत्त का संगायन किया था और इसी पूर्णिमा के दिन वैशाली के चापाल चैत्य में भगवान ने सकल जगत को स्तब्ध कर देने वाली घोषणा की थी- तीन माह बाद तथागत महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होंगे। और माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रैदास का जन्म हुआ है। जन्म भी वहाँ हुआ जहाँ तथागत ने प्रथम धम्मोपदेश किया, वाराणसी में। संत रैदास बुद्ध धम्म की एक धारा हैं। संत रैदास जयंती के अवसर पर दिया गया एक व्याख्यान पुनः उद्धृत कर रहा हूँ।)
संत रैदास बुद्ध धम्म की एक धारा हैं। प्रत्यक्ष रूप से वह बौद्ध नहीं दिखते हैं लेकिन गहन विवेचना उनको सीधे बुद्ध धम्म से जोड़ती है।
उनका जन्म उस समय हुआ, 15वीं शताब्दी में, जब बुद्ध का धम्म भारत से क्रमिक रूप से लुप्त हो हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में उससे नये सम्प्रदायों का जन्म हो रहा था , जो प्रत्यक्ष रूप से नये सम्प्रदाय दिख रहे थे लेकिन उनकी मौलिक जड़ें बुद्ध धम्म में थीं।
बौद्ध धर्म का एक सम्प्रदाय सहजयान बन चुका था। इसी सहजयान से भक्ति सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसके उल्लेखनीय प्रकट व्यक्तित्व मध्यकाल के संत हैं- संत रैदास, संत कबीर उनमें सर्वाधिक विख्यात हैं।
संत रैदास के पदों और दोहों का गहन अध्ययन किया जाए तो वे बुद्ध के वचनों के सिवा कुछ नहीं हैं।
चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु एवं अन्य कुछ लेखकों व शोधार्थियों ने संत रैदास पर लिखित अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है कि:
संत रैदास के पिता का नाम रघु अथवा रघ्घु था और मां का नाम घुरबिनिया अथवा करमा देवी था। इस दम्पति की सारनाथ में प्रवास कर रहे एक बौद्ध भिक्षु भंते रेवत पर बड़ी श्रद्धा थी। वह उनके दर्शन के लिए और उनसे उपदेश सुनने के लिए काशी से सारनाथ प्रायः जाया करते थे। वह निःसंतान दम्पति थे। एक दिन भंते जी ने दान और संतान का माहात्म्य बताया। दान कथा से प्रभावित होकर इस दम्पति ने एक दिन बड़ी श्रद्धापूर्वक अपने गुरु भंते रेवत को भोजनदान दिया और मिष्ठान्न के रूप में खीर खिलाई।
इस भोजनदान के उपरांत यथासमय माता करमा देवी ने एक संतान को जन्म दिया। दम्पति ने अपने गुरु भंते रेवत पर श्रद्धा के कारण बच्चे का नाम रेवतदास रखा जो कि कालान्तर में अपभ्रंशित हो कर रैदास हो गया। इस प्रकार संत रैदास का आध्यात्मिक सम्बन्ध सीधे बुद्ध धम्म से है क्योंकि उनके माता-पिता एक बौद्ध भिक्षु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। यद्यपि कि जब तक रैदास युवा हुए तब तक भंते रेवत शांत हो चुके थे तथापि रैदास के पदों और दोहों में जो शिक्षाएं व्यक्त हुई हैं वह बुद्ध के वचनों के सिवा कुछ भी नहीं हैं:
- रैदास बाम्हन मति पूजिए,जो होवै गुनहीन।
पूजिहि चरन चण्डाल के, जऊ होवै गुन परवीन।। - रैदास उपजई सब एक बूँद ते, का बाम्हन का सूद।
मूरिखजन न जानहिं, सभ मह राम मजूद।। - रैदास इक ही नूर तो, जिमि उपज्यो संसार।
ऊँच-नीच किहि बिधि भये, बाम्हन अरु चमार।। - रैदास जनम के कारने, होत न कोऊ नीच।
नर को नीच कर डारि है, ओछे करम की कीच।।
रैदास के ये वचन ठीक वही हैं जो सदियों पहले बुद्ध ने कहा है :
न जच्चा होति वसलो, न जच्चा होति ब्राह्मणो।
कम्मा होति वसलो, कम्मा होति ब्राह्मणो ।।
– जन्म से कोई अछूत नहीं होता, न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। कर्म से कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से कोई अछूत होता है।
दया भाव हिरदै नहीं,भखहिं पराया मास।
ते नर नरक महं जाइहिं, सत भाषै रैदास। ।
यह भगवान बुद्ध के शिक्षा पद को संत रैदास ने अपने शब्दों में कहा है –
पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि- मैं प्राणिमात्र की हिंसा से विरत रहने की शिक्षा गृहण करता हूँ।
भगवान बुद्ध का शिक्षा पद है-
सुरामेरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि – मैं समस्त मादक पदार्थों से विरत रहने की शिक्षा गृहण करता हूँ।
भगवान बुद्ध के इन्हीं शिक्षा पदों को संत रैदास ने अपने युग में अपनी तरह से कहा है :
रैदास मदुरा का पीजिये,जो चढ़े उतराए।
नांव महारस पीजिये, जो चढ़े नहिं उतराए।।
संत रैदास, संत कबीर एवं मध्यकाल के अनेक संतों के पदों में इष्ट के रूप में, आराध्य के रूप में राम , श्याम, गोविन्द, गिरधर इत्यादि शब्दों का उल्लेख है जिसे पढ़कर बुद्धिवादी लोग रैदास को बौद्ध परम्परा की एक धारा मानने में थोड़ा झिझकते हैं। लेकिन इस झिझक को रैदास के समकालीन उनके धर्मबन्धु संत कबीर ने बड़ी निर्भीकता से तोड़ा है:
राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर अरु चोर।
जो नाम साधु जपे सोई नाम कुछ और ।।
इन संतों के इष्ट राम वह राम नहीं हैं जिस राम के नाम पर आज हाहाकार हो रहा है, दंगा-फसाद हो रहा है। इन संतों के राम उनका अंतर का बुद्धत्व है, निर्वाण है:
संत रैदास ने कहा भी है :
कहि रैदास समुझि रे संतों, इह पद है निरवान।
इहु रहस कोई खोजै बूझै, सोइ है संत सुजान।।
संत रैदास के पदों और भजनों में बड़ी गहन बौद्ध शब्दावलियों का, टर्मिनोलाजी का, प्रयोग हुआ है :
कहि रैदास तजि सभ त्रस्ना…
संत रैदास समस्त तृष्णा को तज देने की बात कर रहे हैं।
भगवान बुद्ध के सम्बोधि के ठीक बाद प्रथम वचन हैं- तन्हानं खय मज्झगा- तृष्णा का क्षय हो गया है…
यह तृष्णा शब्द बौद्ध शब्दावली है। धम्मपद में पूरा एक अध्याय तृष्णा पर है – तन्हा वग्गो अर्थात तृष्णा वर्ग।
वही संत रैदास कह रहे हैं-
कहि रैदास तजि सभ त्रस्ना…
संत रैदास का साधना मार्ग विपस्सना है। विपस्सना का सहज सा अर्थ है समता में रहना- न सुखद वेदनाओं से राग, न दुःखद वेदनाओं से द्वेष, बल्कि समता में स्थित रहना।
संत रैदास वही अनुभूति अपने शब्दों में कहते हैं:
राग द्वेष कूं छाड़ि कर, निह करम करहु रे मीत।
सुख दुःख सभ महि थिर रहिं, रैदास सदा मनप्रीत।।
वे विपस्सना की एक बड़ी गहन अनुभूति को बड़े प्रेमल शब्दों में व्यक्त करते हैं:
गगन मण्डल पिय रूप सों, कोट भान उजियार।
रैदास मगन मनुआ भया, पिया निहार निहार ।।
भगवान बुद्ध ने सुख, दुःख, लाभ, हानि इत्यादि को लोक धर्म कहा है। जो इन लोक धर्मों से अविचल रहता है, उसका मंगल होता है:
फुट्टस्स लोक धम्मेहि चित्तं यस्स न कम्पति।
असोकं विरजं खेमं, एतं मंगलमुत्तमं।।
– जिसका चित्त लोक धर्मों से विचलित नहीं होता, वह शोकरहित, निर्मल होता है, यह उत्तम मंगल है।
इसी को संत रैदास ने अपने शब्दों में कहा है:
सुख दुःख हानि लाभ कौ, जऊ समझहि इक समान।
रैदास तिनहि जानिए, जोगी संत सुजान।।
भगवान बुद्ध का शब्द ‘सति’ अथवा स्मृति ही मध्यकाल के संतों की भाषा में सुरति बन गया है। जिसे भगवान बुद्ध ने सम्यक् स्मृति कहा है उसे ही संत रैदास ने सुरति अथवा सुरत कहा है :
सुरत शब्द जऊ एक हो, तऊ पाइहिं परम अनन्द ।
रैदास अंतर दीपक जरई, घर उपजई ब्रम्ह अनन्द ।।
यह ब्रम्ह अनन्द क्या है? ब्रम्ह विहार ही ब्रम्ह आनन्द है। ब्रम्ह विहार अर्थात मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्खा।
भगवान बुद्ध सम्यक् समाधि को आर्य अष्टांग मार्ग के आठ अंगों में एक अंग बताते हैं। उसी समाधि को संत रैदास अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं:
समाधि थिति संत जन, अपनहु अप्प मिटांहि।
जिमी गंगा समुद मिलि, रैदास समुदहि विलांहि ।।
भगवान बुद्ध धर्म के नाम पर चल रहे अंधविश्वासों के विध्वंसक हैं और संत रैदास उसे पुष्ट करते हैं:
जहं अंध विस्वास है, सत्त परख तहं नांहि ।
रैदास संत सोई जानिहै, जौ अनुभव होहि मन माहि।
भगवान बुद्ध के वचन हैं:
मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया…
– मन समस्त धर्मों का पूर्व नायक है, मन श्रेष्ठ है …
संत रैदास ने इसी बात को अपने समय की भाषा में कहा:
मन ही पूजा मन ही धूप,
मन ही सेऊ सहज सरूप।
और
मन चंगा तो कठौती में गंगा …
मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। संत रैदास बुद्ध के प्रतिनिधि हैं।
संत रैदास का विस्तार सम्पूर्ण भारत है- उनके पद मराठी में अभंगों के रूप में मिलते हैं, राजस्थानी में मिलते हैं, पंजाब में गुरुग्रन्थ साहेब में गुरुमुखी में मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि संत रैदास का विस्तार तिब्बत तक है। बुद्ध धम्म में चौरासी सिद्धों का उल्लेख है। चौरासी सिद्धों का क्रमवार विवरण तिब्बती परम्परा ने संरक्षित किया हुआ है। चौरासी सिद्धों के विवरण में संत रैदास क्रम संख्या चौदह पर हैं। वह विवरण एक और मिथक तोड़ता है कि संत रैदास के गुरु रामानन्द थे। तिब्बती परम्परा उल्लेख करती है कि संत कबीर और संत रैदास के गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम जालंधर नाथ था।
अतः अब संत रैदास को बोधिसत्व रैदास के रूप में स्थापित करने का समय आ गया है।
संत रैदास जी तथागत बुद्ध को अपना गुरु मानते थे ।
तथागत बुद्ध के चारित्रकार है संत रैदास।
संत रैदास जी ने अपने दोहे में कहा है कि
“अजामिल, गज, गणिका, तारी
काटी कुंजीर पाश
ऐसे गुरमते मुक्त किये तू क्यों न तरे रैदास!”
– अजामिल यानि अंगुलिमाल, हे तथागत तुमने अंगुलिमाल जैसे हिंस्र आदमी को इंसान बनाया
हे तथागत तुमने गज यानि पागल हाथी को शांत किया उसके भी मार्गदाता बन गए ।है तथागत गणिका यानि आम्रपाली के आप मार्गदाता बन कर उसका घमंड को चूर चूर करके उसे भिक्खु संघ में लिया।तुम इन सभी के मार्गदाता हो गए, तो तुम्हारे इस रैदास के तुम गुरु नहीं हो ?
संत रैदास बुद्ध को अपना गुरु घोषित किये थे। संत रैदास और संत कबीर अपने दोहे में तथागत बुद्ध को अपना गुरु घोषित किए थे। ब्राम्हण इन बातों को छुपाते है। ताकि हमारी प्रेरणा सही सामने न आये।
संत शब्द भी त्रिपिटक से आया है।
भारत में संतो का जो आंदोलन चल रहा है वह मूलतः बुद्ध धम्म का ही अंग है।